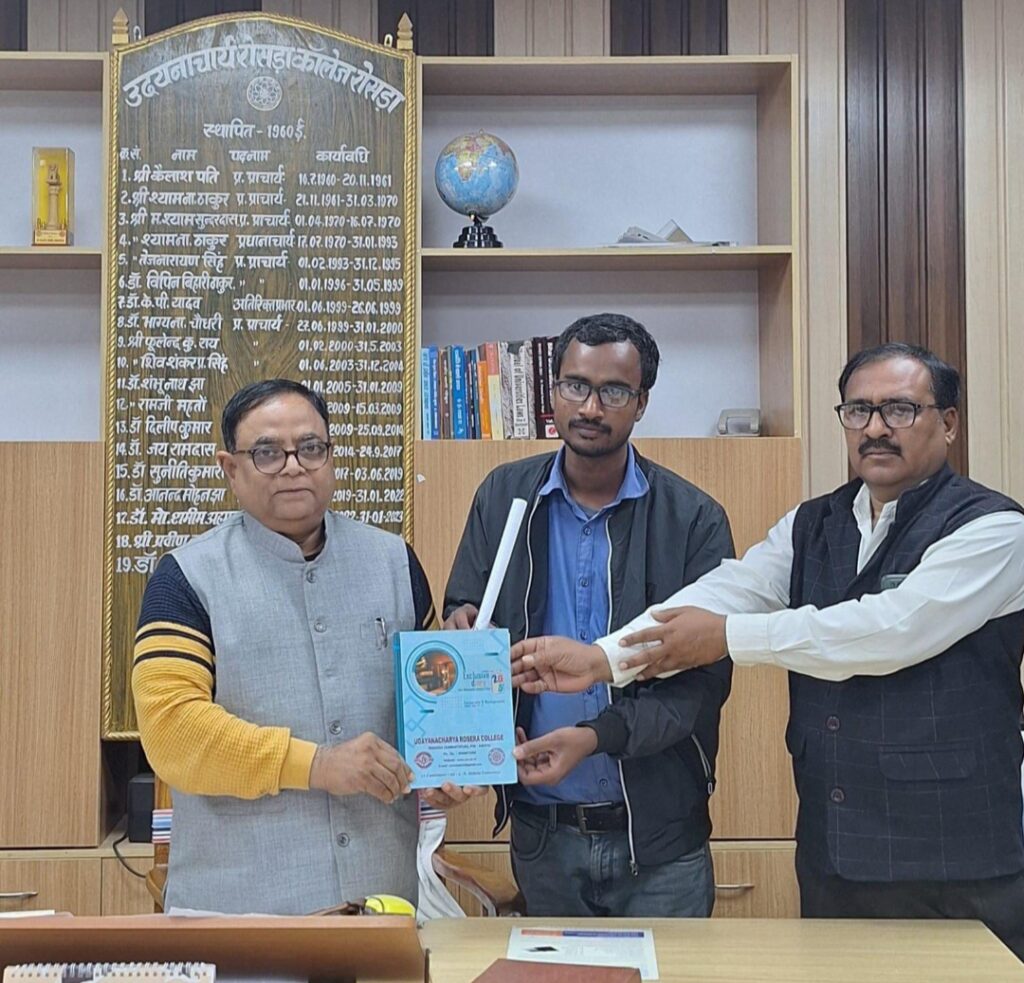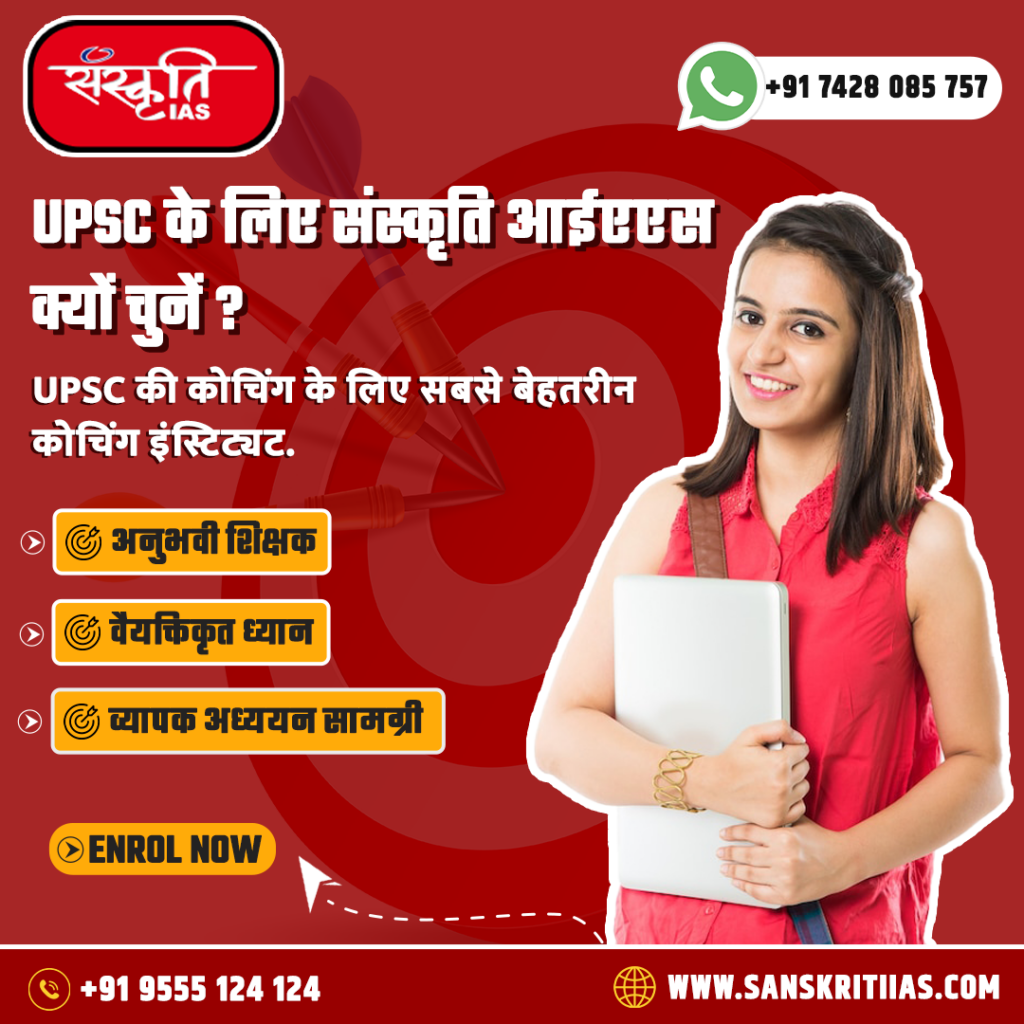दरभंगा (ब्यूरो रिपोर्ट) : बिहार, जो कभी प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का गौरवशाली केंद्र था, आज उच्च शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगीकरण में पिछड़ चुका है। आर्यभट्ट और चाणक्य की यह भूमि, जो कभी ज्ञान और विद्वता का प्रतीक थी, आज उच्च शिक्षा के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बिहार शिक्षा के मामले में देश के 28 राज्यों में अंतिम स्थान पर है।

*ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार*:- बिहार में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) मात्र 14.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 27.1% है। हर साल 5 लाख से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। राज्य में 25% से अधिक स्नातक स्तर की सीटें खाली रह जाती हैं। 13 राज्य विश्वविद्यालयों और 250+ महाविद्यालयों में 50% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 2008 से किसी भी विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई, जिससे पुस्तकालय निष्क्रिय हो चुके हैं।
10% से भी कम विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति कार्यरत हैं, जिससे प्रशासनिक ढाँचा चरमरा गया है।

*यू. आर. कॉलेज, रोसड़ा: उच्च शिक्षा की जमीनी हकीकत*- यू. आर. कॉलेज, रोसड़ा की स्थापना 1960 में हुई और अंगीभूतिकरण 19797 में किया गया। प्रारंभ से वर्तमान तक में सरकार ने कला , विज्ञान और मानविकी के 14 विषयों को मान्यता दी थी जिसकी पढ़ाई स्नातक स्तर पर होती है। पूर्व कुलसचिव घनश्याम राय द्वारा शोधार्थी रुपेश कुमार यादव को दी गई जानकारी के अनुसार, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन शिक्षकों, कर्मचारियों और संसाधनों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई।
*महत्वपूर्ण आँकड़े*:- इतिहास विषय में 1960-62 में मात्र 40 सीटें थीं, जो अब 487 हो चुकी हैं। एक सेमेस्टर में 500 विद्यार्थी मेजर कोर्स में प्रवेश लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ही 3000 विद्यार्थी नामांकित होते हैं। पर्याप्त कक्षाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के अभाव में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

*शिक्षकों की कमी और विषय विशेषज्ञता का संकट*- शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार:- 40% से अधिक विश्वविद्यालयों में नियमित प्रोफेसरों की संख्या 10% से भी कम है। लोक प्रशासन और श्रम एवं सामाजिक कल्याण जैसे विषयों में शिक्षकों का भारी अभाव है।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में लोक प्रशासन विषय में मात्र 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है, जबकि आवश्यक संख्या 15 से अधिक होनी चाहिए। कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से कक्षाएँ या तो बंद हो चुकी हैं या नियमित रूप से नहीं लगतीं।
*उच्च शिक्षा संस्थानों की आधारभूत संरचना की दयनीय स्थिति*- 70% से अधिक कॉलेज किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। 80% से अधिक महाविद्यालयों में वाई-फाई, स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
विश्वविद्यालय परिसरों में 75% पुस्तकालयों में अद्यतन पुस्तकें और डिजिटल संसाधन नहीं हैं। 80% विज्ञान और तकनीकी महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण पुराने हो चुके हैं। छात्रावासों और कैंटीन सुविधाओं की कमी के कारण छात्र नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं कराते।
*तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा: उद्योगों से जुड़ाव का अभाव*- तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास की कमी के कारण बिहार के युवा अन्य राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार:-बिहार में आईटीआई कॉलेजों की संख्या मात्र 260 है, जबकि आवश्यक संख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। राज्य में हर साल 10 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए बेरोजगार रहते हैं। सरकार द्वारा “कुशल युवा कार्यक्रम” और “बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना” जैसी पहल की गईं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इन योजनाओं के तहत मात्र 3,000 युवाओं को ही रोजगार मिल सका, जो कि राज्य की युवा आबादी के मुकाबले नगण्य है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिक्षकों की भारी कमी और आउटडेटेड पाठ्यक्रम के कारण उद्योगों से तालमेल नहीं बन पा रहा है।
*समाधान की दिशा में ठोस कदम* -1. विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में नए शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। 2. शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कम से कम 5 नई कक्षाओं का निर्माण हो। 3. सरकार नियमित निरीक्षण और समीक्षा करे ताकि वास्तविक जरूरतों का आकलन हो सके। 4. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता और अनुदान दिया जाए ताकि आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा सके। 5. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से जोड़ा जाए, ताकि युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलें। 6. शिक्षा बजट में कम से कम 50% की वृद्धि की जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। 7. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं।
*निष्कर्षत*:- बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान और समाज के सभी हितधारकों को मिलकर ठोस प्रयास करने होंगे। अन्यथा, बिहार का युवाजन शिक्षित और रोजगार योग्य होने के बजाय पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझता रहेगा। आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि क्या राजनीतिक दल इस संकट को गंभीरता से लेंगे या फिर यह सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रहेगा?